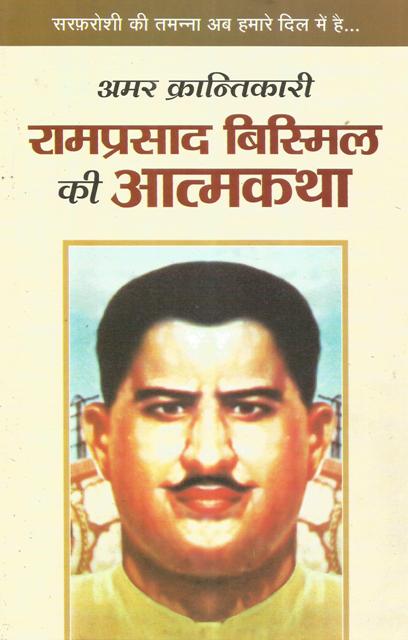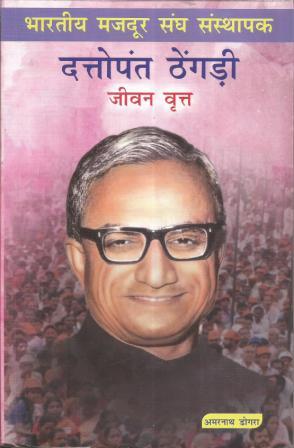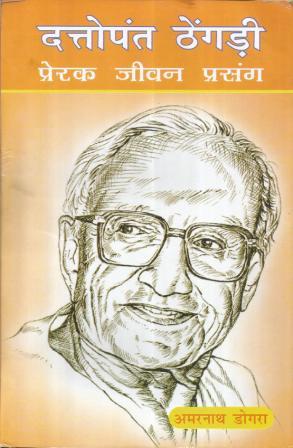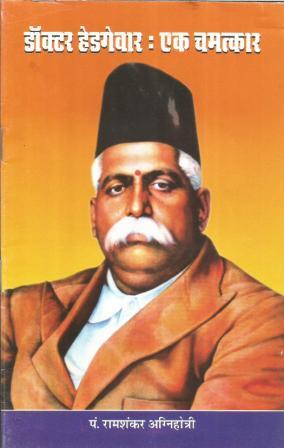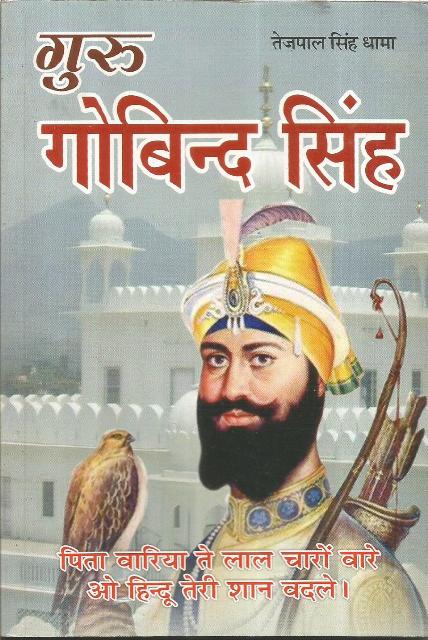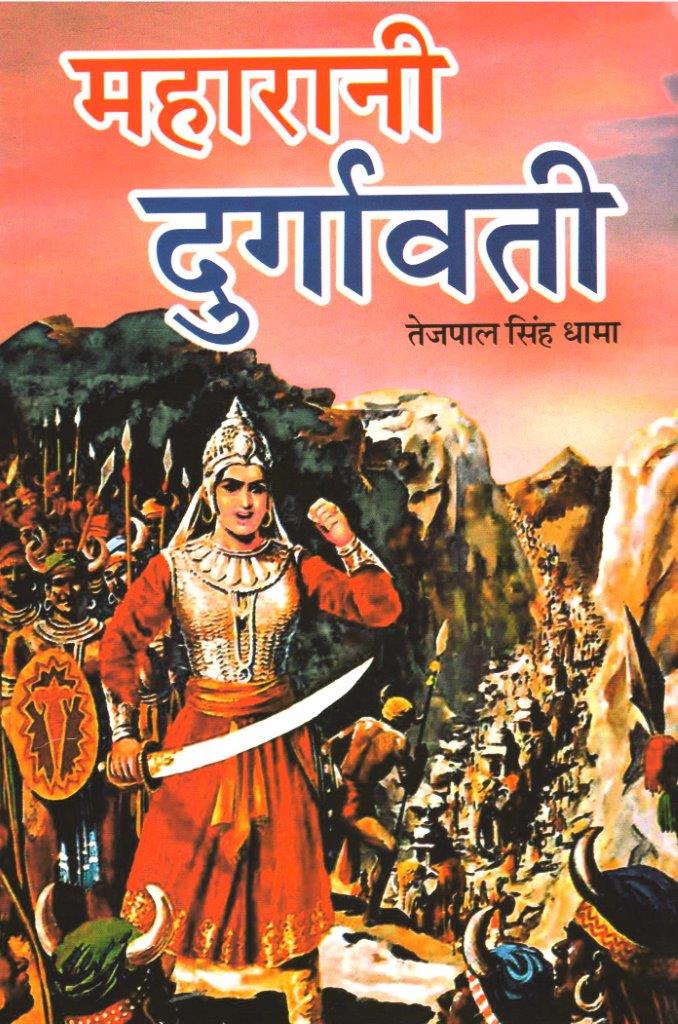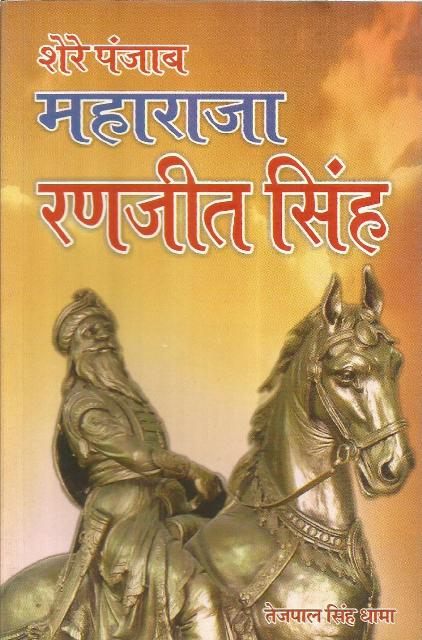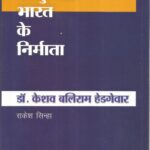
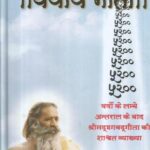
Cash on Delivery available
Ramprasad Bismil Ki Aatmkatha
₹195.00
Ramprasad Bismil Ki Aatmkatha
Shipping & Delivery
-
India Post Parcel Service
India Post Service is now realiable and good service, esay tracking and take prompt action on complains.
8-9 Days
Start From Rs 60
-
Delhivery and Other Private Courier Service
To Avail this service you have to pay extra charges according to your parcel weight.
4-5 Days
Start From Rs 90
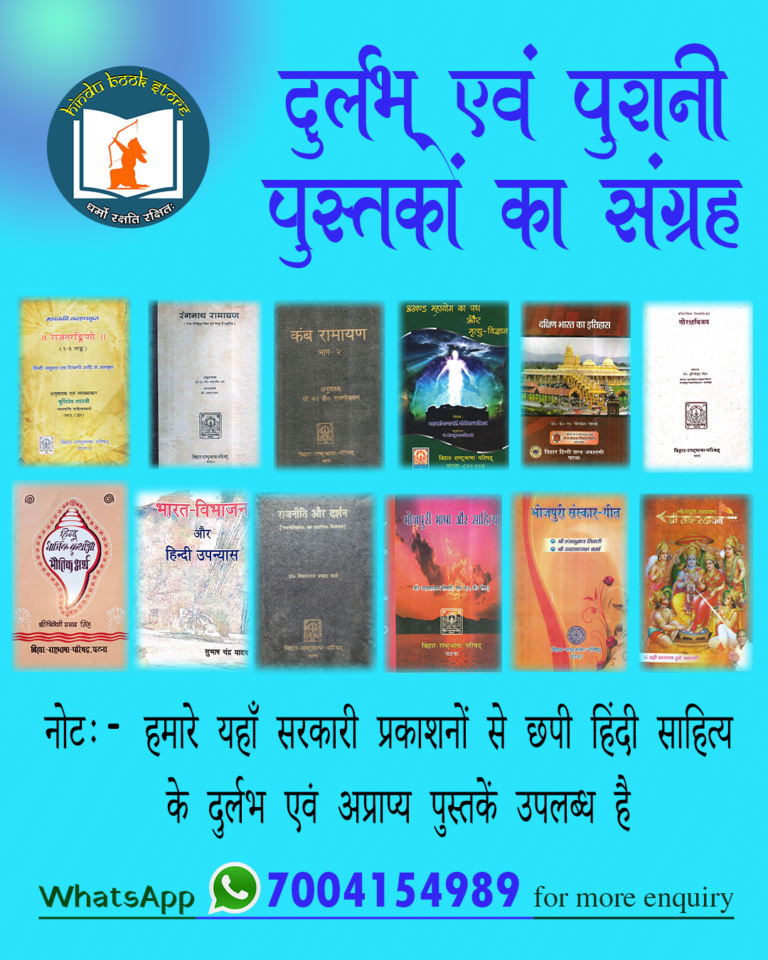
Specification
 Publisher and Writter
Publisher and Writter
| Writer | |
|---|---|
| Publisher |
Description
शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा
भारतीय स्वतंत्रतता आंदोलन का वह दूसरा प्रस्थान बिंदु था जब उत्तर भारत के क्रांतिकारी संगठनकर्त्ताओं योगेशचन्द्र चटर्जी और शचीन्द्रनाथ सान्याल ने मिलकर एक नए अखिल भारतीय क्रांतिकारी दल की रूपरेखा तैयार की और उसका नाम रखा ‘भारतीय प्रजातंत्र संघ । इस दल ने अपनी नीतियों और आदर्शों का एक घोषणापत्र भी जारी किया जिसे ‘पीला पर्चा’ कहा गया। वह गांधी के असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद का समय था जब क्रांतिकारियों ने घोषित किया था कि वे एक ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का और एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण संभव नहीं होगा। स्पष्टतः उस समय के क्रांतिकारी संगठनों ने स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य के साथ ही प्रजातंत्र और शोषणमुक्त समाज की अपनी परिकल्पना को आकार देना शुरू कर दिया था।
इसी संगठन में क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल एक नए नेता के रूप में सामने आए। उनके पास प्रसिद्ध मैनपुरी षड्यंत्र केस (1918-1919) का जीवंत अनुभव था जिसमें उन्हें लंबा और कठिन फरारी जीवन बिताना पड़ा। सरकार की ओर से घोषित आम माफी के बाद वे सार्वजनिक तौर पर प्रकट हुए और काकोरी काण्ड की योजना में लग गए। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ और आलमनगर के मध्य काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट दस नौजवानों के साथ ट्रेन रोककर सरकारी खजाने को हथियाने की उनकी योजना ब्रिटिश सरकार को सीधी चुनौती थी जिसमें हुई धर-पकड़ में वे अपने अनेक क्रांतिकारी साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में आ गए। 18 महीने तक लखनऊ में सरकार बनाम रामप्रसाद’ नाम से चले मुकदमे को तब बहुत प्रसिद्धि मिली थी जिसमें उन्हें अपने तीन अन्य साथियों अश्फाकउल्ला और रोशनसिंह के साथ 19 दिसम्बर 1927 को फांसी क्रमशः गोरखपुर फैजाबाद, इलाहाबाद और गोंडा की जेलों में फांसी पर चढ़ा दिया गया जबकि इस मामले में तीसरे साथी राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी को अकारण ही 17 दिसम्बर को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। अन्य क्रांतिकारियों को लंबी सजाएं मिलीं।
काकोरी की यह घटना भारतीय क्रांतिकारी संग्राम का एक ऐतिहासिक पड़ाव
है। इस अर्थ में भी इसे अपने पूर्ववर्ती क्रांतिकारी युद्ध से सर्वथा पृथक करके देखा
जा सकता है कि पहली बार भारतीय क्रांतिकारियों ने विभिन्न छोटे-छोटे क्रांतिकारी
संगठनों और अपनी छापेमार लड़ाइयों से हटकर अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़े
दल को खड़ा करने की दिशा में मजबूती से अपने कदम बढ़ाए थे और विचार के
स्तर पर देश में शोषणमुक्त जनतंत्र की स्थापना का सपना देखा था। 1921 के
अहसयोग आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम में सर्वथा नए प्रयोग के नाते भारतीय
क्रांतिकारियों ने उसे असीम धैर्य के साथ देखा ही नहीं था, बल्कि उस अवधि के
लिए अपने संघर्ष को विराम भी दे दिया था। भविष्य के अनेक क्रांतिकारी यथा
चन्द्रशेखर आजाद, रोशन सिंह और मन्मथनाथ गुप्त सरीखे नौजवान असहयोग के
सिपाही बन कर ही क्रांतिकारी संग्राम से जुड़े और उन्होंने ऊंचाइयां हासिल की।
लेकिन असहयोग की निराशाजनक समाप्ति के बाद भारतीय राजनीति में जो एक
खालीपन व्याप्त हो गया था, उसे अपने अभियान से भरने में काकोरी की इस घटना
ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसने देश का ध्यान तब साम्प्रदायिकता से संग्राम
की ओर मोड़ा तथा देश की आजादी के लिए नए सिरे से नौजवानों में बलिदान की
भावना को भरने में योगदान दिया। काकोरी शहीदों का बलिदान देश की सर्वाधिक
रोमांचकारी घटना बनी और इस संघर्ष में अशफाकउल्ला की उपस्थिति और
सक्रियता ने उसे ऐसी मिली-जुली शहादत का दर्जा दे दिया जो पूर्व में दुर्लभ था
तथा उसने भविष्य के क्रांतिकारी संग्राम के लिए नई इबारत रच दी। अर्थात
रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्ला भिन्न धार्मिक आस्थाओं के होते हुए देश की
आजादी के लिए एक मार्ग के राही बने। ऐसे में उनके मजहबी आचार-विचार कहीं
बाधक नहीं बने बल्कि यह सवाल ही बहुत दूर बना रहा कि कौन किस सम्प्रदाय
का और यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के रास्ते में धर्म बाधक बनता है तो वे उसे भी एक
ओर रखने में कोताही नहीं करते। बिस्मिल थे आर्यसमाजी और अशफाकउल्ला
मुसलमान। पर दोनों में गजब की दोस्ती। दोनों एक शहर के निवासी । बिस्मिल
के पास क्रांतिकारी संघर्ष का अनुभव था पर अशफाक एकदम नए थे जब वे काकोरी
के अभियान में भाग लेने के लिए आगे बढ़े। वे कोशिश करके क्रांतिकारी दल में
सम्मिलित हुए थे। इसलिए कि उन दिनों उनके धर्म के किसी व्यक्ति की देश क्रांतिकारी संघर्ष में हिस्सेदारी नहीं थी। ऐसे में वे बिस्मिल को बहुत भरोसे में लेकर उस संग्राम से जुड़ सके। वे अपने को साबित करना चाहते थे कि देशभक्ति के लिए बलिदान देने में वे किसी से पीछे नहीं हैं और अंततः उस पूरे अभियान में उन्होंने को एक खरा क्रांतिकारी सिद्ध करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी। बिस्मिल को उन पर नाज था और स्वयं अशफाक भी उन्हें अपना नेतृत्वकर्ता और बड़ा भाई मानते थे।
बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा गोरखपुर के फांसीघर में बैठकर लिखी थी। जहां भी लिपिबद्ध करने के लिए सर्वथा विपरीत परिस्थतियां थी। काल कोठरी की कुछ तंग और तनाव देने वाली तनहाई साम्राज्यवाद की पुलिस का कड़ा पहरा और आंखों के सामने झूलता फांसी का क्रूर फंदा। ऐसे में कुछ भी कलमबंद करना एक निर्भीक, स्थिरचित्त और संतुलित मस्तिष्क का कारनामा ही हो सकता है जिसने गहराई से जीवन का अर्थ समझ लिया हो और जो अपने सम्पूर्ण जीवन ही नहीं बल्कि उस पूरे क्रांतिकारी अभियान को जिसमें उसने दीर्घ अवधि तक सघन हिस्सेदारी की. उसे एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखने-परखने का माद्दा भी रखता हो। रजिस्टर के आकार के कागजों पर पेंसिल से छिपते-छिपाते अपने शब्दों और विचार-श्रंखला को उकेरना गहरे जीवट का काम था। पर बिस्मिल इसमें सफल हुए और अपने लिखे को तीन खेपों में देशभक्त जेल वार्डरों के मार्फत उन्होंने जेल से बाहर गोरखपुर के दशरथ प्रसाद द्विवेदी के पास पहुंचवाया और इस तरह उस क्रांतिकारी की वह आत्मरचना गणेश शंकर विद्यार्थी के पास पहुंची। 19 दिसम्बर बिस्मिल की फांसी का दिन निर्धारित था यानी उस दिन सवेरे ही उन्हें शहादत के मार्ग पर चले जाना था और अपनी इस जीवनकथा को वे 17 दिसम्बर तक लिपिबद्ध करते रहे। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस नई पीढ़ी के लिए भी जिसे भविष्य के क्रांतिकारी संग्राम के सपने ही नहीं बुनने थे अपितु अपने को उस कण्टकीर्ण मार्ग पर चलने का अभ्यस्त भी बनाना था।